योगांग में प्राणायाम स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है और इसके अनेक प्रकार भी हैं। कर्मकांड में भी प्राणायाम का विशेष महत्व है और प्रत्येक कर्म के आरम्भ में प्राणायाम करना आवश्यक कहा गया है। कर्मकांड सीखने वालों के लिये प्राणायाम का योग संबंधी ज्ञान हो अथवा न हो किन्तु कर्मकांड के लिये जो सामान्य विधान है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता मात्र स्वयं हेतु नहीं अपितु यजमानों को सिखाने के लिये भी है।
इस आलेख में कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में प्राणायाम का महत्व, प्राणायाम की विधि व अन्य अनेकों तथ्यों का वर्णन किया गया है।
कर्मकांड में प्राणायाम विधान – pranayama kya hai
अंतर्जाल पर प्राणायाम के बारे में वैसा लेख जो कथित वैज्ञानिक हो सरलता से दिखेगी किन्तु शास्त्रोक्त चर्चा का अभाव ही है। यदि आप प्राणायाम की शास्त्रोक्त चर्चा ढूंढें तो कठिनता से ही कोई आलेख प्राप्त होगा। वास्तव में अंतर्जाल के आभासी दुनियां में सनातन शास्त्रों के प्रति दुराग्रह है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि शास्त्रोक्त चर्चा को जानबूझ कर दबाया जाता है, छुपाया जाता है। अन्यथा प्राणायाम ढूंढने पर अधिकतर शास्त्रोक्त चर्चा वाले आलेख ही मिलने चाहिये थे। कर्मकांड सीखें पर शास्त्रोक्त चर्चा की ही आवश्यकता है।
गीताऽध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च ॥
उपरोक्त श्लोक में बताया गया है कि गीता के अध्ययन में लगे रहने वाले और प्राणायाम पारायण के शरीर में पाप शेष नहीं रहता है। उसमें एक और विशेषता भी बताई गयी है कि इस जन्म के पाप की तो चर्चा ही क्या करें, पूर्व जन्म के पापों का भी नाश होता है।
उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः। स्नात्वा विप्रो दिग्वासा प्राणायामेन शुद्ध्यति॥
उष्ट्रयान (ऊंट की सवारी) खर (गधे की सवारी), यदि ब्राह्मण जानबूझकर ऊंट या गधे की सवारी करे, नग्न होकर स्नान करे तो प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। सोचने का विषय है कि वैज्ञानिक अवधारणा से ऊंट, गधे की सवारी करने से, नग्न स्नान करने से किस दोष की सिद्धि होगी। और यही कारण है कि ये आधुनिक सोच रखने वाले और वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने वाले श्वान के साथ शयन करने में भी कोई दोष नहीं समझते।
गाय की सेवा, संरक्षण, संवर्द्धन में इन्हें भले ही साम्प्रदायिकता दिखती रहे, पिछड़ा सोच दिखे, पुराना जमाना दिखे।
जो पूर्व व पर जन्म को ही नहीं स्वीकारता हो, पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं जानता हो उसके द्वारा कर्मकांड/धर्म सम्बन्धी किया गया विश्लेषण कैसे ग्राह्य हो सकता है। जिसने कभी चन्दन लगाया ही न हो वो चन्दन का क्या विश्लेषण करेगा ?
ये लोग कभी धोती धारण नहीं करते, परिधान से अंग्रेज बने रहते हैं और व्याख्या सनातन के विषयों की करते हैं तो कितना सही कर सकते हैं। यदि सनातन का तनिक भी ज्ञान हो तो प्रथम परिधान से सनातनी दिखना प्रारंभ करेंगे और जो इतना भी नहीं जानता वो सनातन के विषयों का ज्ञाता कैसे सिद्ध हो सकता है ?
प्राणायाम क्या है
प्राणायाम = प्राण + आयाम करते हुये विभिन्न प्रकार के शब्दार्थ संबंधी विश्लेषण व्याकरण का विषय है, उसी प्रकार योग में प्राणायाम की भिन्न चर्चा व अनेकानेक प्रकार भी पाये जाते हैं। हम यहां व्याकरण अथवा योग के दृष्टिकोण से प्राणायाम की चर्चा नहीं करेंगे। यहां कर्मकांड विषयक चर्चा होती है इस लिये कर्मकांड के दृष्टिकोण से ही प्राणायाम की चर्चा करेंगे।
प्राणोवायुरितिप्रोक्तः आयामस्तन्निरोधनं। प्राणायाम इतिप्रोक्तो योगिनां योगसाधनं ॥
यद्यपि ऊपर के श्लोक में योग और योगी का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु यह योग उस योग से भिन्न है जो दूरदर्शन आदि पर देखने को मिलता है। विभिन्न माध्यमों से जो योग हम नित्यप्रति देखते हैं वो आध्यात्मिक फल से रहित प्रकार है। उसमें मात्र स्वास्थ्य संबंधी विमर्श ही किया जाता है और प्रचार करने के उद्देश्य से तो प्रणव आदि का त्याग भी कर दिया गया है, जिससे साम्प्रदायिकता का लांछन न लगे।
तथापि इसका एक अन्य पहलू भी है और वो यह कि प्रणव में सबका अधिकार नहीं है अस्तु प्रणवरहित प्रचार-प्रसार ही युक्ति-युक्त है।
प्राण को वायु कहा जाता है और वायु में भी एक वायु का नाम प्राणवायु है। आयाम के अनेकार्थों में विस्तारीकरण ही प्रमुखतया ग्रहण किया जाता है किन्तु यहां निरोध बताया गया है “आयामस्तन्निरोधनं”। निरोध का अर्थ तो बाधित करना ही, व्यवधान उत्पन्न करना ही होता है और प्राणायाम में बाधित ही किया जाता है। एक बार वायु को ग्रहण करके बाधित किया जाता है और पुनः वायु का त्याग करके बाधित किया जाता है अर्थात दोनों बार रोका जाता है।
प्राणायामैस्त्रिभिः पूतो गायत्रीं तु ततो जपेत् । प्राणस्य वायोरायामो निरोधः प्राणायामः ॥ – संवर्त्त के वचन में भी निरोध का भाव ही प्राप्त होता है। प्राण की वायु अथवा प्राणवायु का निरोध करना प्राणायाम है।
प्राणवायु का निरोध करना ही प्राणायाम कहा गया है जो योगियों के योग का साधन होता है। योगियों के योगसाधन में विशेष प्रकार का निरोध होता है जो अल्पकालिक ही नहीं दीर्घकालिक भी होता है। इससे आगे बढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि प्राणवायु का निरंतर प्रवाह या आवागमन होता रहता है अर्थात प्राण में स्थिरता का अभाव होता है। निरोध का तात्पर्य प्राण को स्थिर करना ही है और इस प्रकार प्राणायाम का तात्पर्य प्राण को स्थिर करना है।
विभिन्न कथाओं से भी ज्ञात होता है कि योग में स्थित व्यक्ति आहार आदि ही नहीं साँस का त्याग करके भी दीर्घकाल तक योगावस्था में ही स्थित रहते थे।
सामान्य मनुष्य बिना स्वास लिये १० मिनट भी जीवित नहीं रह सकता और योगी बिना स्वास लिये सहस्रों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, इसका तात्पर्य है कि प्राणायाम के माध्यम से प्राण को शरीर में स्थिर कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राणायाम का तात्पर्य होता है प्राण को स्थिर करने का अभ्यास। प्राणायाम प्राण को स्थिर करने का अभ्यास मात्र ही है।

कर्मकांड में प्राणायाम की आवश्यकता
प्राणायाम की आवश्यकता को प्राणायाम के महत्व के माध्यम से ही समझा जा सकता है और यह महत्व भी शास्त्रोक्त हो तब।
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित् ॥
व्यास के इस वचन में बताया गया है कि व्याहृति-प्रणव युक्त सशिर गायत्री का जो नित्य जप करते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। यह बहुत ही बड़ी विशेषता है और प्राणायाम के महत्व को ही प्रकट करता है।
व्यास – षोडशाक्षरकब्रह्म गायत्र्यास्तु शिरस्स्मृतम् । सकृदावर्तयान्विप्रः संसारात्सविमुच्यते ॥
यथा पर्वतधातूनां दोषान्दहति पावकः । एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते ॥
जैसे पर्वत और धातुओं के दोषों को अग्नि जला देता है वैसे ही अन्तर्गत पापों को प्राणायाम जला देता है – अर्थात प्राणायाम से पापों का नाश होता है और शुद्धता की सिद्धि होती है जो किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व अनिवार्य होता है।
त्वक् चर्ममांसरुधिरमेदोमज्जास्थिभिः कृताः । तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात् ॥ – अत्रि
कौन-कौन से पाप नष्ट होते हैं इसकी व्याख्या अत्रि के वचन से प्राप्त होती है – इन्द्रियों और साथ ही त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि आदि का दोष प्राणायाम करने से भस्म हो जाता है । अर्थात प्राणायाम के द्वारा शरीर के सभी कोशों में स्थित पापों/दोषों/अशुद्धियों का निवारण होता है।
आ केशाग्रान्नखाग्राच्च निरोधश्शक्यते बुधैः । निरोधाज्जायते वायुर्वायोरग्निश्च जायते ॥ अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तश्शुद्धयते त्रिभिः ॥ पुनः अत्रि और स्पष्ट करते हुये कहते हैं केश-से-नख पर्यन्त निरोध करने में जो बुद्धिमान सक्षम हो जाता है, निरोध से वायु उत्पन्न होता है, उस वायु से अग्नि और पुनः अग्नि से जल उत्पन्न होता है, तत्पश्चात इस विधि को तीन बार करने से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है।
एवं सम्मार्जनं कृत्वा वाह्यशुद्धयर्थकारकम् । अथाभ्यन्तरशुद्धचर्थं प्राणायामं समाचरेत् ॥
योगयाज्ञवल्क्य का कथन है कि सम्मार्जन (पवित्रीकरण) बाह्य शुद्धि करता है, भीतरी शुद्धता के लिये प्राणायाम करना चाहिये। अर्थात जब भी हम कोई कर्म करने के लिये प्रवृत्त होते हैं तो शुद्धिकरण प्रथम आवश्यकता है और बाह्य शुद्धि तो विभिन्न प्रकार स्नान, मार्जन आदि से प्राप्त की जाती है किन्तु भीतरी शुद्धि के लिये प्राणायाम करना आवश्यक होता है।
य एता व्याहृतीस्मप्त संस्मरन्प्राणसंयमे । उपासितं भवेत्तेन विश्वं भुवनसप्तकम् ॥
सर्वेषु चैव लोकेषु कामचारश्च जायते ॥ – योगयाज्ञवल्क्य
प्राणायाम के लाभ
योगयाज्ञवल्क्य – प्राणायामत्रयं कृत्वा सूर्यस्योदयनं प्रति । निर्मलास्स्वर्गमायान्ति मन्तस्मुकृतिनो यथा ॥
प्राणायाम की आवश्यकता को समझने से ही प्राणायाम से होने वाले लाभ का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राणायाम का तात्पर्य शरीर की आंतरिक शुद्धि सिद्ध होती है, पापों का शमन सिद्ध होता है और इन्हीं दोनों आधारों से प्राणायाम से होने वाला लाभ भी स्पष्ट होता है।

आंतरिक शुद्धि : आंतरिक शुद्धि का तात्पर्य है विकारों का निवारण, विकारों से तात्पर्य षड्विकार हैं। मनुष्य के पतन का कारण ये षड्विकार ही होते हैं और यदि प्राणायाम से विकारों का शमन होता है तो इसका तात्पर्य है कल्याण प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात प्राणायाम के लाभ में यह भी कहा जा सकता है कि इसके आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
पापों का शमन : शास्त्रों में प्राणायाम से पापों का निवारण भी कहा गया है। दुःख-रोग आदि के कारण पाप ही होते हैं अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो दुःख, व्याधि, दरिद्रता आदि पापों के ही फल होते हैं। और प्राणायाम से पापों का शमन होता है अर्थात दुःख-दारिद्रय-व्याधि आदि का भी निवारण होता है।
यम – दशप्रणवसंयुक्तैः प्राणायामैश्चतुर्दशैः । मुच्यते ब्रह्महत्यायाः किं पुनश्शेषपातकैः ॥
वैज्ञानिक तर्क गढ़ने वाले अन्य प्रकार से स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ बतायेंगे किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता धर्म के विषय में है ही नहीं, ये आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही इसकी व्याख्या की जानी चाहिये।
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥
संवर्तोऽपि – मानसं वाचिकं पापं कायेनैव तु यत्कृतम् । तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रं प्राणायामत्रये कृते ॥
मनु के अनुसार विधिवत तीन प्राणायाम जो व्याहृति-प्रणव से संयुक्त हो उसे ब्राह्मण के लिये परम तप समझना चाहिये। जैसे तपाने से धातुओं के मल का नाश होता है और धातु शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार इन्द्रियों के दोष का प्राणायाम से शमन होता है।
अब यह उत्तम फल तो तभी सिद्ध हो सकता है जब उस भ्रांतिमूलक वैज्ञानिक अवधारणा मात्र को धर्म/अध्यात्म में ग्रहण न किया जाय, शास्त्र वचन को ग्रहण किया जाय। किन्तु इसके विपरीत यदि शास्त्रवचन का त्याग करके वैज्ञानिक अवधारणा स्वास्थ्य लाभ को ग्रहण किया जाय तो शास्त्रोक्त फल कि सिद्धि भी नहीं हो सकती, किन्तु अन्य शास्त्रोक्त प्रमाणों से अत्यल्प फल भी तब प्राप्त होगा जब व्याहृति-प्रणव आदि का प्रयोग किया जाय।
वैज्ञानिक अवधारणा में तो सर्वग्राह्यता का भाव ग्रहण करके व्याहृति-प्रणव आदि का त्याग ही किया जा रहा है अथवा उसे अनावश्यक सिद्ध किया जा रहा है।
सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥
मनु जी ने ही आगे और कहा है “प्रणव युक्त व्याहृतियों से सोलह प्राणायाम करने से भ्रूणहत्या जैसे पापों का भी एक मास में शमन हो जाता है, साथ ही नित्य के पाप तो नित्य ही समाप्त हो जाते हैं” यह वचन अतिविशेष है और इसकी एक विशेषता यह भी है कि अन्य वचनों को अधर्मी/नास्तिक/वैज्ञानिक अवधारणा से ग्रसित व्यक्ति ग्रहण तो नहीं करेगा किन्तु इसे अवश्य ग्रहण करेगा।
मनु के इस वचन का तात्पर्य यह है कि प्राणायाम करने वाले का बड़े-से-बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है और नित्य के पाप तो नित्य ही नष्ट होते हैं। किन्तु यह वचन पाप के लिये प्रेरित करने वाला नहीं है अपितु इसका उचित अर्थ पाप से बचना है, और यदि पाप हो भी जाये तो उसका निवारण हो जायेगा। नित्य-पाप तो दैनिक-जीवन में नित्य होते ही रहते हैं, उसमें अनावश्यक भ्रम न रखे।
अधर्मी/पापी/नास्तिक/वैज्ञानिक अवधारणा रखने वालों के लिये विपरीतार्थ : प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शास्त्र वचनों के ही विपरीतार्थ भी ग्रहण किये जाते हैं, विपरीत व्याख्या भी की जाती है। मनु के इस वचन की अधर्मी/पापी/नास्तिक/वैज्ञानिक अवधारणा से ग्रसित व्यक्ति विपरीतार्थ ही ग्रहण करेगा। इसका विपरीतार्थ पाप की प्रेरणा है, “पापों का शमन होता है अतः पाप करने से मत बचो, पाप करो और उसके शमन के लिये प्राणायाम कर लो” यह विपरीतार्थ है।
प्राणायाम कब करना चाहिए
प्राणायामैर्विना यद्यत्कृतं कर्म निरर्थकम् । अतो यत्नेन कर्तव्यः प्राणायामः शुभार्थिना ॥ – अगस्त्य
प्राणायाम के बिना जो भी कर्म किया जाता है वो सभी निरर्थक हो जाता है; अतः प्राणायाम किसी भी पूजनादि के आरम्भ में अनिवार्य रूप से करे । अगस्त्य के इस वचन में प्राणायाम को सभी कर्मों में अनिवार्य बताया गया है, सभी कर्मों का तात्पर्य नित्य-नैमित्तिक और काम्य तीनों प्रकार के कर्म होते हैं। “प्राणायामैर्विना” प्राणायाम से रहित होने पर “यद्यत्कृतं कर्म निरर्थकम्” जो भी कर्म किया गया हो वह निरर्थक होता है।
अर्थात प्रत्येक कर्म की सार्थकता हेतु प्राणायाम अनिवार्य है। वर्त्तमान में सभी कर्मों से प्राणायाम का विलोप होते देखा जा रहा है जो चिंता का विषय है। यह वचन उस स्थिति में भी पालनीय है जब किसी पद्धति से कोई कर्म कराया जा रहा हो और उस पद्धति में प्राणायाम का उल्लेख न किया गया हो।
जैसे सत्यनारायण पूजा विधि, रुद्राभिषेक विधि, उपनयन-विवाह आदि पद्धतियों में प्राणायाम का उल्लेख नहीं प्राप्त होता, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्राणायाम अनिवार्य है और पद्धति में उल्लेख हो वा न हो करना ही चाहिये।
Discover more from कर्मकांड सीखें
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







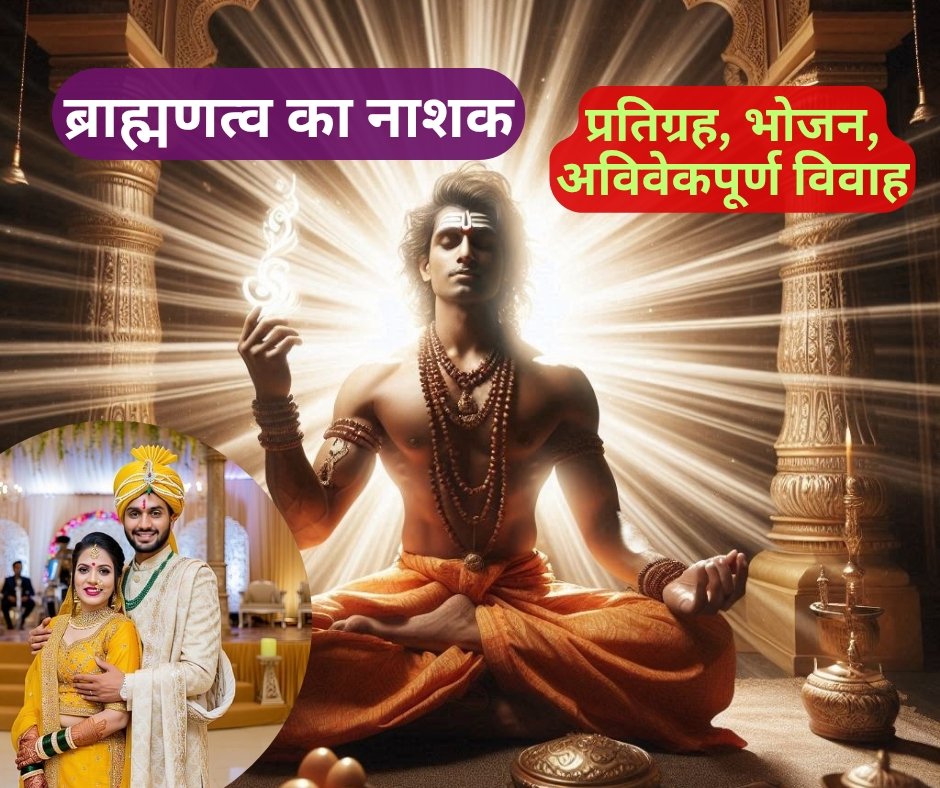
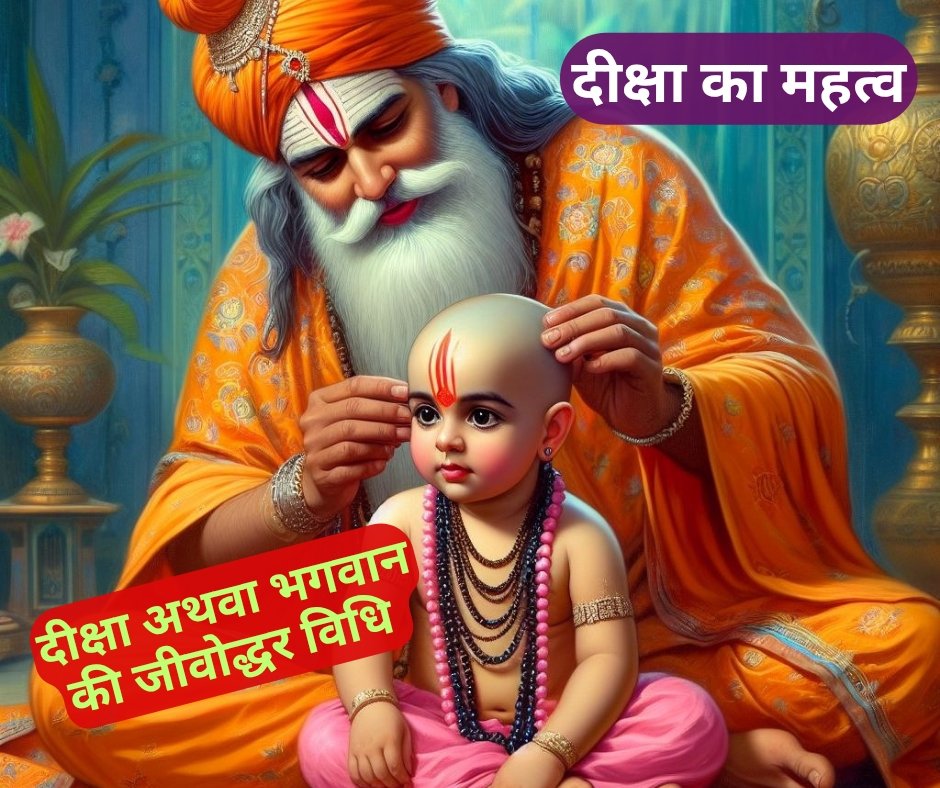
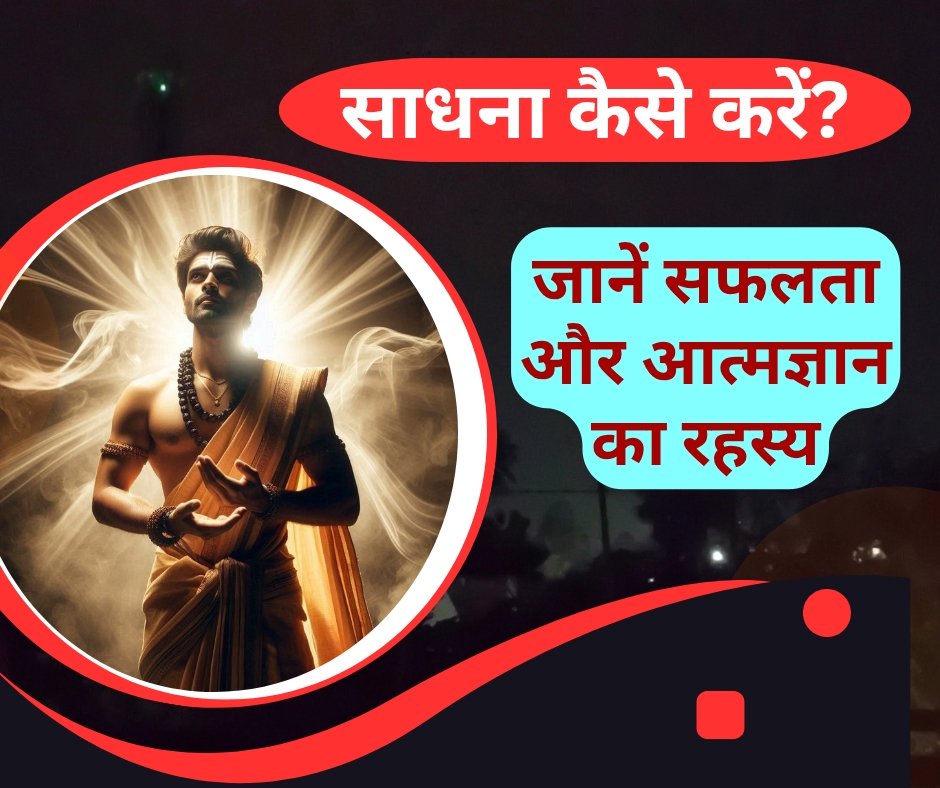

One thought on “कर्मकांड में प्राणायाम विधान – pranayama kya hai”