आप कर्मकांडी हैं या बनना चाहते हैं तो आपको पग-पग पर प्रमाण की आवश्यकता होती है और यदि प्रमाण न हो तो किसी कथन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। किसी विषय पर आपके वक्तव्य का महत्व तभी हो सकता है जब आपके पास प्रमाण हो। किन्तु आप कर्मकांडी होकर कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण शब्द बोलेंगे तो अगला व्यक्ति कर्मकांड की परिभाषा पूछ देगा। उसे इस विषय से कोई लेना-देना नहीं होगा कि कर्मकांड के विषय में प्रमाण की पृथक व्याख्या होगी। वो प्रमाण की परिभाषा न्यायदर्शन के अनुसार बतायेगा और यदि आप तदनुसार उत्तर नहीं देंगे तो आपको शीघ्र ही मूर्ख सिद्ध कर देगा।
पूर्व आलेख में कर्मकांड सीखने हेतु प्रमाण संग्रह करने की बात कही गयी थी किन्तु संग्रह करने से पूर्व प्रमाण को जानना समझना भी आवश्यक है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण की जानकारी हो, परिभाषित कर सकें, प्रमाण के प्रकारों की व्याख्या कर सकें एवं ये भी बता सकें कि कर्मकांड में प्रमाण का क्या तात्पर्य है।
प्रमाणसंग्रहण : ले लो प्रमाण नहीं तो पग-पग पर ठेस लगेगी
यह घोषित है कि कर्मकांड सीखें वेबसाइट कर्मकांड से संबंधित चर्चा करता है, कर्मकांडी पंडित भी कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करते हैं। संभवतः इस पर विश्वास न हो और इसके लिये उदाहरण देना आवश्यक है; प्रायः एक कर्मकांडी दूसरे से मतभिन्नता होने पर प्रमाण देने के लिये कहते हैं :
- उस समय प्रमाण का क्या तात्पर्य होता है ?
- क्या न्याय दर्शन की परिभाषा के अनुसार अनेकानेक प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं ?
एक कर्मकांडी द्वारा प्रमाण की अपेक्षा पर दूसरे कर्मकांडी द्वारा शास्त्रों के वचन दिये जाते हैं। ये पुराण, स्मृति, सूत्र आदि ग्रंथों के होते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मकांड में तर्क-अनुमान आदि कुछ भी प्रमाण नहीं माना जाता है। तर्क व अनुमान द्वारा जो सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है उसी के समर्थन में प्रमाण की अपेक्षा की जाती है और तर्क-अनुमान आदि के समर्थन में शास्त्र-वचन प्रस्तुत न कर पायें तो उसकी सिद्धि नहीं होती।
ऊपर जो चर्चा की गयी है इसके लिये भी प्रमाण की आवश्यकता होगी, किन्तु ऐसा निरंतर होता है, और इसका प्रमाण है ग्रंथों में भी सदा यही विधा अपनायी जाती है। दो विद्वान एक ही विषय पर भिन्न मत (वक्तव्य/आलेख) प्रस्तुत करते हैं और समर्थन में शास्त्रों के वचन प्रस्तुत करते हैं। फिर एक विद्वान ऐसे भी होते हैं जो दोनों में तारतम्य स्थापित करते हुये निष्कर्ष निकालते हैं। इन सभी क्रियाओं में क्या प्रमाण होता है ? शास्त्रों के वचन, जिसे न्याय में शब्दप्रमाण कहा जाता है।
किन्तु कर्मकांड में यह शब्द प्रमाण रूप से प्रमाण का एक प्रकार नहीं होता अपितु सम्पूर्ण प्रमाण ही शब्द प्रमाण होता है। एक कर्मकांडी दूसरे कर्मकांडी से प्रमाण में इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात कर्मकांड में प्रमाण का तात्पर्य यदि न्याय के प्रमाणवत ग्रहण किया जाय तो कोई विषय सिद्ध ही न हो पाये अथवा अनेकानेक सिद्धियां हो जो एक-दूसरे का विरोधाभाषी भी होगा।
आगे की चर्चा पर आगे बढ़ने से पूर्व यह स्पष्ट करना पूर्ण आवश्यक है कि कर्मकांड सीखें पर अथवा कर्मकांडी न्याय दर्शन के धरातल पर विमर्श नहीं करता। न्याय एक भिन्न व स्वतंत्र विषय है जो दर्शन का अंग है। और जिसे न्याय के धरातल पर प्रमाण संबंधी चर्चा की अपेक्षा हो वो न्याय पढ़े, नैयायिक बने, कर्मकांडी नहीं। यदि न्याय के आधार पर कर्मकांड सम्बन्धी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाय तो ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे जीवविज्ञानी भूविज्ञान के सूत्रों से जीवविज्ञान का विमर्श करना चाहे।
प्रमाण क्या है अथवा प्रमाण की शब्द व्युत्पत्ति
प्रमाण विषयक चर्चा मुख्य रूप से न्याय दर्शन में है। किन्तु षड्दर्शन में प्रमाण विषयक चर्चा है, प्रमाण की व्याख्या है। षड्दर्शन हैं : पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक।
प्रमाण की विभिन्न अवस्थाएँ और उनके उपयोग का विवेचन इन दार्शनिक विचारधाराओं में मिलता है। पूर्व मीमांसा, जो वेदों की व्याख्या और तर्क की शक्ति को मानती है; उत्तर मीमांसा, जो ज्ञान और तर्क के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप को समझती है; सांख्य, जो संख्या और तत्वों के माध्यम से जगत की उत्पत्ति और क्रम को स्पष्ट करती है; योग, जो मानसिक और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताती है; न्याय, जो तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य के ज्ञान में अग्रसर है; और वैशेषिक, जो पदार्थों के गुण और उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करती है।
- पूर्वमीमांसा में जैमिनी ने प्रमाण के तीन प्रकार, प्रभाकर ने पांच और कुमारिल भट्ट ने छह प्रकार बताये हैं।
- वेदांत दर्शन में छह प्रकार के प्रमाण को स्वीकार किया गया है : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि।
- सांख्य दर्शन में तीन प्रकार के प्रमाण बताये गये हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द (आप्त)
- वैशेषिक दर्शन में दो प्रकार के ही प्रमाण स्वीकार किये गये हैं : प्रत्यक्ष और अनुमान।
- न्याय दर्शन में प्रमाण के चार प्रकार बताये गये हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द।
न्याय दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और एक कालखंड ऐसा भी था जब न्याय को जानने वाला ही विद्वान माना जाता था, यदि न्याय का ज्ञान न हो तो विद्वान नहीं माना जाता था। न्याय, जो तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की प्राप्ति संबंधी विश्लेषण करता है अर्थात न्याय दर्शन; प्रमाण के बारे में भी विशेष जानकारी प्रदान करता है। किन्तु जहां कर्मकांड सीखने की चर्चा हो रही हो और यह भी कठिन हो वहां दर्शन की चर्चा विषय से भटकना होगा।
साथ ही साथ नैयायिक नहीं हूँ यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करता हूँ अर्थात स्वीकारता हूँ। क्या मैं रसायनशास्त्री हूँ, नहीं हूँ तो समस्या क्या है ? क्या मैं जीववैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक हूँ, नहीं। नहीं हूँ तो इसमें समस्या क्या है और इसे स्वीकारने में क्या समस्या है। उसी प्रकार कर्मकांडी यदि ज्योतिषी नहीं है तो उसे स्वीकारने में समस्या नहीं होनी चाहिये, और यदि नैयायिक नहीं है तो भी। दोषी वो कर्मकांडी है जो नैयायिक होने का भ्रमोत्पन्न करके कर्मकांडी से प्रमाण का न्याय संबंधी ज्ञान पूछता है, एवं न्याय संबंधी अत्यल्प व्याख्यान ही प्रस्तुत करते हुये स्वयं को ज्ञानी कर्मकांडी को अज्ञानी सिद्ध करता है।
वैसे इस विषय में आपलोग स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिये, दर्शनशास्त्र से प्रमाण की चर्चा करनी चाहिये अथवा कर्मकांड में प्रमाण का तात्पर्य समझना चाहिये। यदि दर्शन की चर्चा करने लेंगे तो न कर्मकांड सीखने में सहयोग प्राप्त होगा न ही दर्शन का ज्ञान, भटकते रह जायेंगे। कर्मकांड सीखें पर कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण की चर्चा करनी ही अपेक्षित है जो कर्मकांड सीखने में अधिक सहयोगी हो।
प्रमाण का तात्पर्य
भले ही न्याय दर्शन के अनुसार कर्मकांड में प्रमाण की चर्चा न की जाय किन्तु इतना अवश्य है कि प्रमाण का तात्पर्य समझना आवश्यक है। “प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्” अर्थात् जिससे प्रमा की प्राप्ति/सिद्धि हो उसे प्रमाण कहते हैं । “प्रमाकरणं प्रमाणं” से जो प्रमा करे वह प्रमाण है। इसमें प्रमाकरण लक्षण है और प्रमाण लक्ष्य है। प्रमा का करण अर्थात साधन प्रमाण कहलाता है।
पुनः “प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणं” ; अब प्रमा की चर्चा करें तो कहा गया है “यथार्थानुभः प्रमा” यथार्थ का अनुभव/सत्य का ज्ञान प्रमा है। इस प्रकार यथार्थ अर्थात सत्य का ज्ञान प्रमा है और जिस माध्यम से प्रमा की प्राप्ति हो, साधित हो वह करण/साधन है, एवं जो करण अर्थात साधन करे, सिद्ध करे वह प्रमाण है।

कर्मकांड में उपरोक्त विभिन्न प्रकार के प्रमाणों में से शब्द (आप्त) प्रमाण लिया जाता है। कर्मकांड मात्र शब्द (आप्त) प्रमाणधारित विधा है। प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण कर्मकांड में स्वीकार्य नहीं है।
- शिव-विष्णु-दुर्गा-राम-कृष्ण का प्रत्यक्ष, अनुमान आदि से ज्ञान प्राप्त करते हैं अथवा शब्द (आप्त) प्रमाण ?
- वर्षपर्यंत विभिन्न व्रत-पर्वों का निश्चय करते हैं, किस प्रमाण से करते हैं – शब्द (आप्त) प्रमाण से।
- शांतिकर्म करना है इसमें कौन सा प्रमाण प्राप्त होता है – शब्द (आप्त) प्रमाण।
- नित्यकर्म करना है इसमें कौन सा प्रमाण प्राप्त होता है – शब्द (आप्त) प्रमाण।
- नैमित्तिककर्म करना है इसमें कौन सा प्रमाण प्राप्त होता है – शब्द (आप्त) प्रमाण।
- काम्यकर्म करना है इसमें कौन सा प्रमाण प्राप्त होता है – शब्द (आप्त) प्रमाण।
अब शब्द और आप्त को भी संक्षेप में समझना आवश्यक है, क्योंकि इसे समझे बिना कर्मकाण्ड में प्रमाण का तात्पर्य समझना कठिन होगा। क्योंकि कर्मकांड में शब्द (आप्त) ही प्रमाण है।
- शब्द प्रमाण : आप्त का उपदेश शब्द (शब्द प्रमाण) कहलाता है; आप्तोपदेशः शब्दः (न्यायसूत्र 1.1.7)।
- आप्त : धर्म का साक्षात्कार करने वाला वह वक्ता जिसने सत्य को जाना और सत्य को यथार्थ शब्दों में व्यक्त किया आप्त कहलाता है। पदार्थ/विषय का साक्षात्कार प्राप्त होना आप्ति है, उसमें प्रवृत्त होने वाला आप्त है और आप्त द्वारा प्राप्त उपदेश शब्द (प्रमाण) है – आप्तोपदेशः शब्दः (न्यायसूत्र 1.1.7)।
प्रमाण की परिभाषा
इससे विस्तृत चर्चा की आवश्यकता कर्मकांड में तो नहीं होती है। कर्मकांड में प्रमाण का तात्पर्य कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय करने हेतु, अर्थात क्या विहित है, क्या अविहित है, विहित काल, निषिद्ध काल, प्रक्रिया, क्रम इत्यादि का ज्ञान/निर्धारण/निश्चय करना पड़ता है। इन सबका निर्धारण/निश्चय स्वेच्छा, अनुभव अथवा अन्य किसी प्रकार से नहीं किया जाता, मात्र एक प्रकार से ही किया जाता है और वो प्रकार है श्रुति/स्मृति/पुराण/सूत्रादि ग्रंथों द्वारा। अर्थात कर्मकांड में प्रमाण का एक ही तात्पर्य होता है और वो है उपरोक्त ग्रंथों के वचन।
इसके साथ ही इनकी महत्ता इतनी है कि यदि शास्त्रोक्त तथ्य प्रस्तुत किये बिना वक्तव्य/निर्देश दिया जाय, अर्थात जिसकी शास्त्र से सिद्धि न की जा सके ऐसा कथन करने, निर्देश देने वाला ब्रह्मघातक कहा गया है : “प्रायश्चित्तं चिकित्सा च ज्योतिषे धर्मनिर्णयं। विनाशास्त्रेण यो ब्रूयात् तमाहुर्ब्रह्मघातकं॥” नारद पुराण पूर्व० १२/६४; पायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष, धर्मनिर्णय आदि में बिना शास्त्र के (अर्थात शास्त्र द्वारा जिसकी सिद्धि न हो) कहना/बताना ब्रह्महत्या के समान दोष प्रदायक है।
इस विषय के एक सर्वोत्तम उदाहरण है ज्योतिष का कालसर्प योग। कालसर्प योग के विषय में शास्त्रोक्त प्रमाण कोई प्रस्तुत नहीं कर पाते। ऊपर “प्रायश्चित्तं …….. तमाहुर्ब्रह्मघातकं॥” जो श्लोक दिया गया है वो स्वयं एक शास्त्रवचन अर्थात प्रमाण है और प्रमाण की महत्ता स्थापित करने के लिये है।
कर्मकांड; धर्मनिर्णय में आ जाता है अर्थात कर्मकांड से संबंधित किसी कथन, वक्तव्य, निश्चय, उपदेश आदि करने के लिये शास्त्रसम्मत होना आवश्यक है। शास्त्रसम्मत होने का तात्पर्य है कि कर्मकांड का प्रमाण शास्त्र ही है।
परिभाषा : जिन साधनों के द्वारा असत्य का खंडन और सत्य की प्राप्ति/ज्ञान हो उसे प्रमाण कहा जाता है – “येन साधनेन मिथ्यात्वस्य खण्डनं; सत्यं च लभ्यते/ज्ञानं भवति तत् प्रमाणं कथ्यते”
कर्मकाण्ड में प्रमाण की परिभाषा : कर्मकाण्ड में किसी विषय यथा; कर्तव्याकर्तव्य, विहित-निषिद्ध, काल, विधि, इत्यादि के वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह ज्ञान हम शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड में प्रमाण का तात्पर्य शास्त्र (शास्त्रों के वचन) ही है। “कर्मकाण्डे यः कोऽपि विषयः यथा; कर्तव्याकर्तव्यानां, विहित-निषेधस्य, काल, विधि आदीनां वास्तविकं ज्ञानम् आवश्यकं भवति, एतत् ज्ञानं वयं शास्त्रेभ्यः प्राप्नुमः। एवं कर्मकाण्डे प्रमाणार्थः शास्त्रं (शास्त्रवचनम्)”
In rituals, actual knowledge of any subject such as duty and non-duty, prescribed and prohibited, time, method, etc. is required and we get this knowledge from the scriptures. Thus, in rituals, the meaning of proof is the scriptures.
हम लोगों को व्रत करते देख उनके अनुसार ही व्रत के बारे में धारणा बना सकते हैं, यथा व्रत के दिन भोजनादि का त्याग किया जाता है, अगले दिन पारण किया जाता है, ब्राहण को सीधा (आटा, चावल, सब्जी, दाल आदि भोजन सामग्री) दिया जाता है। किन्तु इसमें अनेकों तथ्य हैं जो छूट गये अर्थात सत्य का ज्ञान नहीं हुआ।
सत्य का ज्ञान हमें शास्त्रों में व्रत विषयक चर्चा से प्राप्त होगा; यथा : व्रत के पूर्व दिन एकभुक्त करे, भूमि पर शयन करे, व्रत के दिन प्रातः काल नित्यकर्म करके व्रतधारण करे, कर्मकाल में व्रत के देवता की पूजा-कथा-दान-हवन आदि करे, निशाजागरण करे, अगले दिन नित्यकर्म संपन्न करके पारण करे, ब्राह्मण भोजन कराये व दान-दक्षिणादि से संतुष्ट करे इत्यादि।
शास्त्राणां ज्ञानं जीवनस्य विविध परिस्थितिषु उचित मार्गदर्शनं प्रदास्यति। यदा वयं कर्मकाण्डं विधाय, तदा शास्त्रवचनानां अनुसरणं न केवलं कर्मफलस्य सिद्धिः ददाति, किन्तु हृदयस्य शुद्धता च वर्धयति, यः वयं धर्मानुसारं जीवनं यापनस्य मूलभूत तत्वम् अस्ति।
ऊपर प्रमाण के संबंध जो चर्चा की गयी है उसके अतिरिक्त कर्मकांड में प्रमाण हेतु एक अन्य विषय भी है जिसका शास्त्र अनुमोदन तो करता है किन्तु इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित ?
आचार-व्यवहार-परम्परा
एक ऐसा काल भी था जब सभी क्षेत्रों में धर्माचरण ही व्यावहारिक जीवन का अंग था, और मिथिला उसका अग्रणी था एवं इसी कारण याज्ञवल्क्य का कथन है “धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिलाव्यवहारतः”
धर्मस्य निर्णयो से तो यह सिद्ध होता है कि यह भी (व्यवहार) प्रमाण के समान ही है और विशेषरूप से मिथिला का व्यवहार। यद्यपि व्यवहार, आचार, परम्परा आदि की शाब्दिक व्याख्या भिन्न हो सकती है तथापि कर्मकांड में सबका भाव समग्र ही होता है। जहां भिन्न अर्थ प्रकट करना हो वहां कुलाचार आदि समानार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुलाचार कथन का तात्पर्य कुल-वंश विशेष का व्यवहार होता है, जो मिथिला व्यवहार का बोधक नहीं होता है। कुछ अन्य विषय भी हैं जो व्यवहार को प्रमाण की मान्यता देने में अवरोध उत्पन्न करते हैं :
- वर्त्तमान में तो मिथिला के कर्मकांडी भी अंग्रेज बनकर (सर्ट-पैंट पहनकर) भटकते रहते हैं, तो क्या इसे भी मिथिला का व्यवहार समझकर प्रमाण स्वीकार कर लेना चाहिये ?
- अधिकांश लोगों ने नित्यकर्म का त्याग कर दिया है तो क्या इस व्यवहार को भी प्रमाण स्वीकार कर लेना चाहिये ?
- सर्वत्र विवाहकाल में वर धोती धारण करना छोड़ रहा है, तो क्या इसे भी भविष्य में प्रमाण स्वीकार किया जायेगा ?
आचार-व्यवहार-परंपरा आदि का पालन सर्वत्र होता है और उसे भी प्रमाण ही माना जाता है, किन्तु मिथिला का विशेष रूप से उल्लेख करने का तात्पर्य है कि जब प्रमाणों-व्यवहारों में विरोधाभास हों तो निर्णय मिथिला के व्यवहार से लेना चाहिये। इसे भी कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझना होगा :
बलि पर सर्वत्र विवाद चलता रहता है और वर्त्तमान काल में वह विवाद मिथिला में भी होने लगा है, अनेकानेक मंदिरों में बलि बंद कर दिया गया है। जबकि मिथिला में प्राचीन काल से बलि का विधान है और यही प्रमाण अन्यों के लिये ग्राह्य है। मिथिला का ये व्यवहार कैसे ? क्योंकि शास्त्रों में बलि को लेकर परस्पर विरोधाभासी वचन भरे पड़े हैं। सर्वत्र विवाद की स्थिति है, अतः निर्णय मिथिला का व्यवहार करेगा। ये अलग विषय है कि निर्णय मिथिला का व्यवहार करेगा तो मैथिलेत्तरों ने मिथिला के व्यवहार को ही परिवर्तित करना आरंभ कर दिया और उलटी गंगा बहा रहे हैं, जिससे ज्ञान लेना चाहिये उसे बलि रोकने का ज्ञान दे रहे हैं।
इसी प्रकार मत्स्य-भक्षण का भी विषय है जिस पर मिथिला का व्यवहार ही निर्णय देता है। किन्तु याज्ञवल्क्य के वचन का तिरष्कार करते हुये मैथिलेत्तर मैथिलों के लिये मछखोर, मच्छीखोर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में विरोधाभास हो तो हो, मिथिला का व्यवहार यदि मत्स्यभक्षण को निर्दोष सिद्ध करता है तो यही निर्णय है, यही प्रमाण है।
इसी प्रकार जैसे जितिया में परस्पर विरोधाभासी प्रमाण प्राप्त होते हैं तो उसका निर्णय/निष्कर्ष मिथिला के व्यवहार से जानना चाहिये। मिथिला के व्यवहारानुसार यदि द्वितीय दिन औदयिक अष्टमी प्रदोषकाल में व्याप्त न हो तो पूर्व दिन सप्तमीसहिताष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। यद्यपि कुछ लोग मिथिला में भी उदयाष्टमी को ही ग्रहण करते हैं किन्तु ये मिथिला का व्यवहार नहीं अपितु कुछ लोगों की कुलपरम्परा है।
पूजन-हवन में “समर्पयामि”, “न मम” आदि का प्रयोग न करना मिथिला का व्यवहार है अर्थात यही निर्णय है, यही प्रमाण है। ये भिन्न तथ्य है कि मिथिला के भी नये कर्मकांडी जिन्हें ज्ञात नहीं है, अथवा अन्य क्षेत्रों से अध्ययन करके आते हैं वो समर्पयामि और न मम का भी प्रयोग करने लगे हैं।
ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं, जहां मिथिला का व्यवहार भी प्रमाणतुल्य ही है और ये घोषित करने वाले स्वयं याज्ञवल्क्य हैं। संभवतः समझने कठिनता नहीं होगी कि कौन सा व्यवहार धर्मनिर्णय का प्रमाण देगा और कौन नहीं ! किसी भी प्रकार के नये व्यवहार उस श्रेणी में नहीं मान्य होंगे, भले ही पूरी मिथिला में बलि बंद क्यों न हो जाये, मत्स्यभक्षण बंद क्यों न हो जाये। इसका निर्णय मिथिला का वो प्राचीन व्यवहार ही करेगा, नया व्यवहार निर्णय नहीं करेगा। इसी प्रकार किसी कुल/वंश अथवा ग्रामविशेष का कोई विशेष व्यवहार निर्णय हेतु ग्राह्य नहीं हो सकता है।
नये कर्मकांडियों के लिये सावधानी
आपको दर्शन, ज्योतिष आदि अन्य विषय का अध्ययन नहीं करना चाहिये ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, किन्तु जब कर्मकांड सीखना ही समस्या है, इसमें भी बाधा है तो आगे अन्य विषयों का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। इस विषय को समझने हेतु पूर्व आलेख का भी अध्ययन करें तब ज्ञात होगा कि कर्मकांड सीखने में भी कैसी समस्यायें हैं। अस्तु जब आप प्रमाण संग्रहण करते हुये कुशल कर्मकांडी बनने का प्रयास करेंगे तो अनेकों कर्मकांडी ही जो स्वेच्छाचारी होंगे समूहबद्ध होकर आपकी टांगे खींचना प्रारंभ करेंगे और ये पंक्ति मेरा स्वयं का अनुभव है।
जब आप एक ऐसे कर्मकांडी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जो कि प्रमाण को महत्व देता हो, इसी प्रकार के वक्तव्य देंगे तो स्वेच्छारियों को ये तथ्य समझ में भी नहीं आयेगी किन्तु इतना अवश्य समझ आयेगा कि भविष्य में आप उनकी दुकान के लिये खतड़ा बन सकते हैं और इसी कारण वो सभी आपके विरुद्ध समूहबद्ध होंगे। नाना प्रकार के कुप्रयास करेंगे, नाना प्रकार के विषयांतर करने वाले प्रश्न करके उलझाने का भी प्रयास करेंगे। किन्तु आपने यदि प्रमाणों का संग्रहण किया है तो आपको डिगा नहीं पायेंगे, यदि आपके पास प्रमाणों का अभाव होगा तो टिकना कठिन होगा।
जब आपसे प्रमाण संबंधी परिभाषा आदि पूछी जाय तो उस समय मौन रहकर विरोधी को ही ज्ञान बघारने का अवसर दें। वो विरोधी जिसने कि कर्मकांड को स्वेच्छाचार बनाकर रख दिया है अधिक नहीं बोल पायेगा। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की परिभाषा करेगा, प्रमाण के चार प्रकार बतायेगा। आप उससे चारों प्रकार का विश्लेषण करने के लिये कहें, जब विश्लेषण कर दे तो कर्मकांड में चारों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने कहें। कर्मकांड में चारों प्रकार प्रयुक्त ही नहीं होता और वह कोई उदाहरण नहीं दे पायेगा और यदि कुछ मनगढंत दे भी दे तो आपकी बारी होगी असिद्ध करने की।
प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष अनुभव होने से प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान सदा यथार्थ हो यह आवश्यक नहीं है। अनेकों विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखेगा कि वर ने धोती धारण नहीं किया, क्या वह प्रमाण हो सकता है ? अधिकांश लोगों ने विधिरहित हवन करना आरंभ कर दिया है, यह प्रत्यक्ष दिखने वाला व्यवहार प्रमाण नहीं हो सकता। श्राद्ध में पहले पाक बनाया जाता है पीछे नित्यकर्म से आरंभ करके श्राद्ध किया जाता है किन्तु यह प्रमाण नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष में तो स्वेच्छाचार किया जाता है उसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार कर्मकांड में प्रत्यक्ष से प्रमाण प्राप्त नहीं होता है।
सूर्योदय-सूर्योदय का जो गणितागत समय होता है वह प्रत्यक्ष में नहीं दिखता। जब तक सूर्य को उदित प्रत्यक्ष न देख लें क्या तब तक वार परिवर्तन नहीं होगा। यदि ओस आदि के कारण अत्यधिक विलम्ब हो तो क्या सूर्योदय नहीं स्वीकार करें और सूर्योदय से आरम्भ होने वाले कर्म न करें। सूर्योदय-सूर्यास्त कर्मकांड का प्रमुख निर्धारक विषय है, इसकी सिद्धि न तो प्रत्यक्ष, न ही अनुमान, न ही उपमान से होती है। एक बार के लिये अनुमान सिद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है किन्तु सूर्योदय सूर्यास्त अनुमान से ज्ञात नहीं होता।
अनुमान
एक यजमान के यहां हवन करते समय स्विष्टकृद्धोम हेतु चरु निर्माण किया गया, यह देखने वाला दूसरे हवन में भी ऐसा अनुमान लगा सकता है, किन्तु दूसरा हवन आज्यमात्र से किया गया, वहां चरुनिर्माण नहीं होगा। अनुमान निरर्थक, शब्दप्रमाण से ही सिद्धि।
उपमान
कर्मकांड में उपमान भी प्रमाण नहीं होता है। नवग्रह शांति विधि से मूल-गण्डांत शांति का उपमान नहीं होता है, और यदि उपमान लगायें तो यथार्थ नहीं होगा। कुण्ड में हवन करने की विधि से वेदी पर हवन करने की विधि का उपमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुंड में नाभि, मेखला, कंठ, योनि आदि होती है जो वेदी में नहीं होती। कुण्ड निर्माण करने के उपरांत वास्तुवेदी निर्माण भी आवश्यक होता है किन्तु वेदी में नहीं। वृद्धिश्राद्ध भी पार्वणविधि से ही करनी चाहिये किन्तु उपमान से यथार्थज्ञान नहीं होगा क्योंकि अनेक अंतर होता है।
- स्नान करते समय देवता-ऋषि आदि जल की आशा से साथ जाते हैं, इसका कौन सा प्रमाण प्राप्त होता है ?
- पितृपक्ष में पितरगण यमपूरी (पितृलोक) से भूलोक पर अपने-अपने वंशजों के यहां आते हैं, इसका कौन सा प्रमाण है ?
- कार्तिक कृष्ण अमावास्या को पितृपक्ष में आने वाले पितर प्रस्थान करते हैं, उल्कादर्शन कराकर उनका मार्गदर्शन कराया जाता है, इसका कौन सा प्रमाण है ?
इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न हो सकते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा और ऐसे लोगों से पूछना होगा। अंत में जब कर्मकांड विषयक अन्य प्रमाण का उदाहरण प्रस्तुत न कर सके, तो समझायें शब्द (आप्त) प्रमाण ही कर्मकांड में पूर्ण प्रमाण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्मकाण्ड में शास्त्र ही प्रमाण है और एक कर्मकांडी दूसरे कर्मकांडी से किसी विषय पर जब प्रमाण की मांग करता है तो संबंधित विषय के शास्त्रोक्त वचन ही दिया जाता है।
किन्तु जो प्रमाण प्रस्तुत न कर सकें, जिनके पास प्रमाण का अभाव हो वो प्रमाण के विषय पर अन्यत्र भटकाने का प्रयास करेंगे, कर्मकांड का ज्ञान नहीं और दर्शन शास्त्र के दर्शन कराने लगेंगे। ऐसे लोग ही प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि प्रमाण को कर्मकांड में भी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। शब्द प्रमाण का अभाव होने पर किसी स्वेच्छाचारी द्वारा किये गये को प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह सिद्ध करेंगे। नयी पद्धतियों को भी शास्त्र ही सिद्ध करेंगे और उसमें की गयी संपादक की टिपण्णी को भी प्रमाण बतायेंगे, किन्तु वेद-पुराण-स्मृति-सूत्र-तंत्र आदि कोई भी शास्त्रोक्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेंगे।
सारांश : कुल मिलाकर यदि आप गुरुकुल में अध्ययन करके कर्मकांडी बन रहे हैं तो भी प्रमाणों का संग्रहण आपके पास होना चाहिये किन्तु इसके लिये आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु यदि आप गुरुकुल में अध्ययन नहीं कर पाये हैं किन्तु कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो आपको प्रमाण संग्रह करने हेतु परिश्रम करना होगा। बिना प्रमाण संग्रह किये आप कुशल कर्मकांडी न तो बन सकते हैं न कभी किसी विषय की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मकांड में प्रमाण का तात्पर्य शब्द (आप्त) ही होता है।
कर्मकांड विधि में शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ प्रामाणिक चर्चा की जाती है एवं कई महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा पूर्व भी की जा चुकी है। तथापि सनातनद्रोही उचित तथ्य को जनसामान्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक बड़ा वैश्विक समूह है जो सनातन विरोध की बातों को प्रचारित करता है। गूगल भी उसी समूह का सहयोग करते पाया जा रहा है अतः जनसामान्य तक उचित बातों को जनसामान्य ही पहुंचा सकता है इसके लिये आपको भी अधिकतम लोगों से साझा करने की आवश्यकता है।






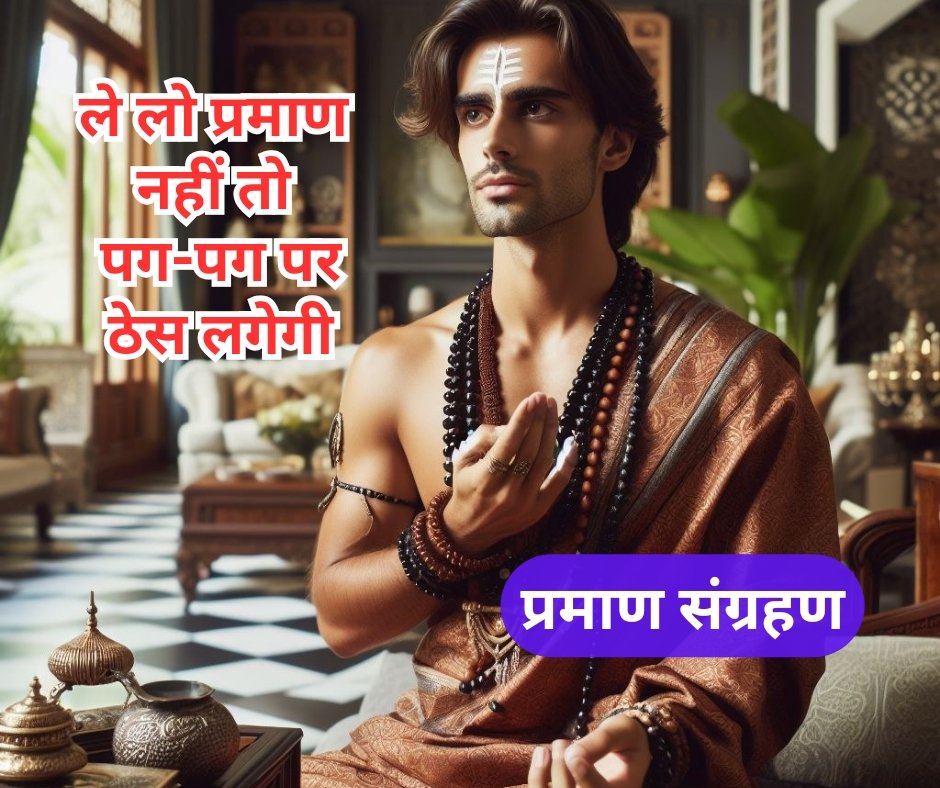










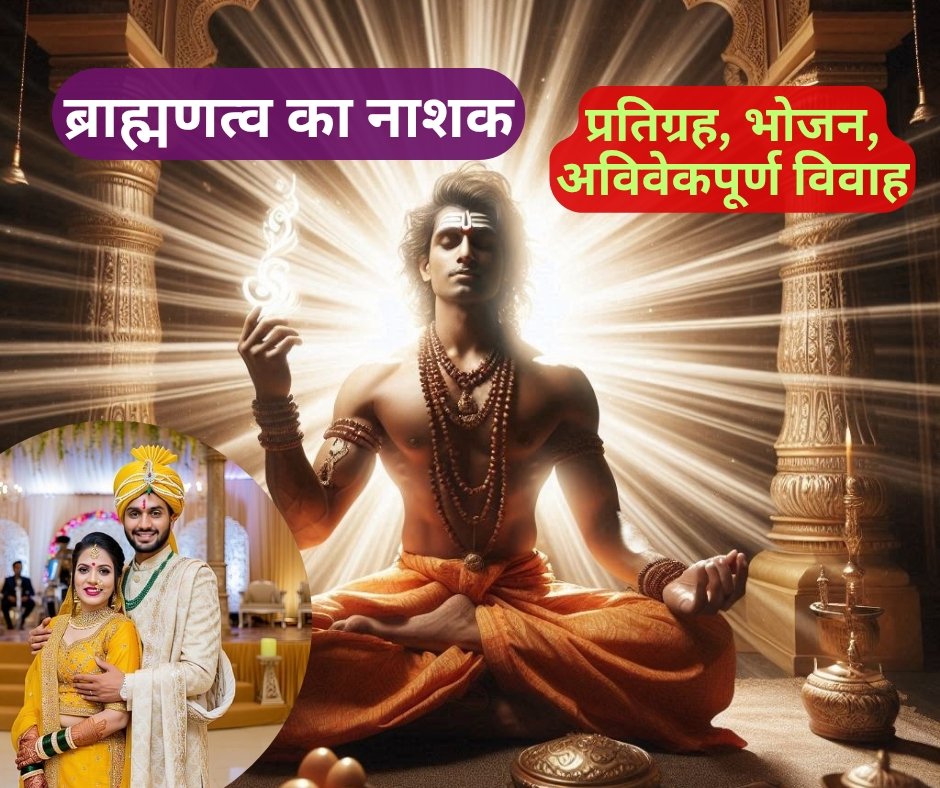
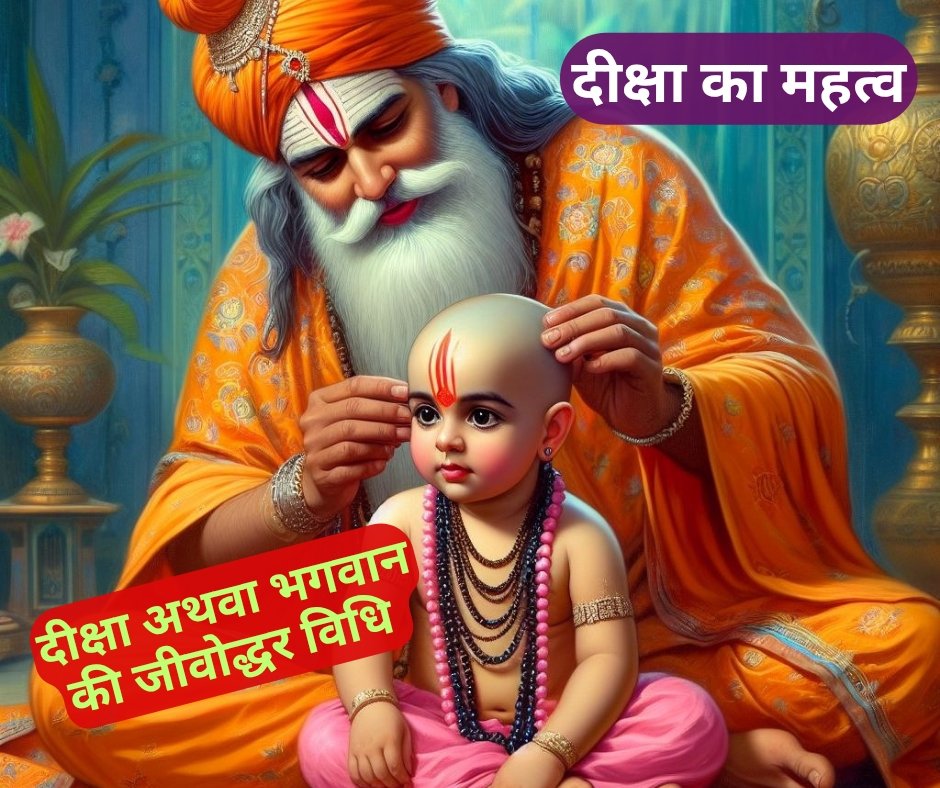
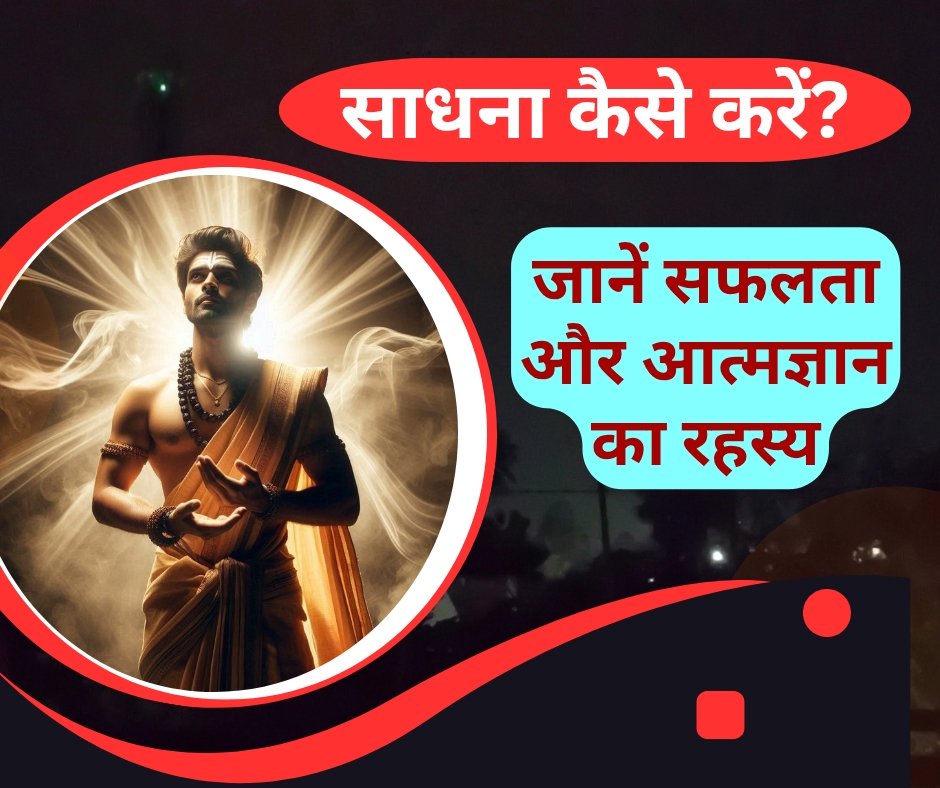

23 thoughts on “प्रमाणसंग्रहण : ले लो प्रमाण नहीं तो पग-पग पर ठेस लगेगी”