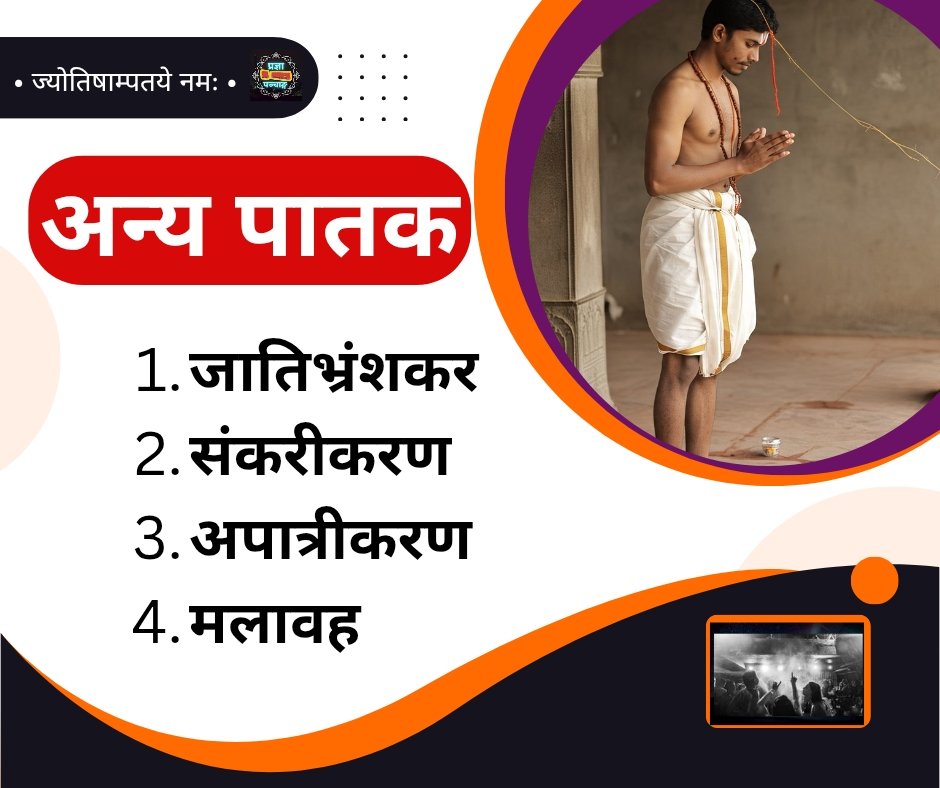रीति के साथ रिवाज़ जोड़कर बोल दिया जाता है जबकि रिवाज़ रस्म के साथ जुड़ा है। इसी प्रकार अब तो विवाह के आमंत्रण पत्रों में स्वागत संदेशों में सर्वत्र शादी का भी बहुत ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम गंभीरता से विचार करें तो ज्ञात होगा कि हमारे पास परम्परा है, विधि विधान है। इसके साथ ही परंपरा और विधान में अंतर भी है। यदि आप कर्मकांडी बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक समझना आवश्यक है और तदनुसार प्रयोग करना।
यदि आपको कर्मकांडी बनना है तो इन्हें अच्छी तरह से समझें : रस्म रिवाज परम्परा प्रथा और विधि विधान
यहां हम परम्परा और विधान की चर्चा करेंगे किन्तु जब परम्परा की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से लोग रस्म, रिवाज़ आदि शब्द का भी प्रयोग करने लगते हैं जैसे मेंहदी रस्म, हल्दी रस्म ये तो पोस्टर लटकाकर, कार्ड बांटकर बताया जाता है। किन्तु जब आप पुनर्जागरण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपको शब्द, भाषा आदि से संबंधित जागरण की आवश्यकता होगी और यदि आप यहां आकर यह कहें कि शब्दों का कोई महत्व नहीं होता किसी भी भाषा का हो तो फिर मंत्रों का क्या महत्व है, स्तोत्रों का क्या महत्व है ?
शब्द का महत्व
हमें यह ज्ञात है कि एक बड़ा गिरोह है जो सनातन के विरुद्ध लम्बे काल से षड्यंत्र कर रहा है और वैसे गिरोह से द्वारा भ्रमित किये गये लोग तपाक से बोलेंगे कि परंपरा कहो या रिवाज़ बात एक ही है। ठीक है बात एक ही है शादी, मैरीज, विवाह कुछ भी कहो एक ही है तो फिर शादी और मैरिज के साथ तलाक, divorce भी जुड़ा है किन्तु विवाह के साथ तो ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है।
इसका प्रभाव भी होता है, विवाह करने वाले तलाक सामान्यतः सम्बन्ध विच्छेद नहीं करते थे, विशेष परिस्थितियों में ही त्याग किया जाता था और रामायण के प्रसंग का स्मरण कीजिये जब सीता को वनवास देने के बाद भगवान राम यज्ञ कर रहे थे तो उसी सीता की प्रतिमा बनायी गयी। विवाह जन्म-जन्मांतर का संबंध होता है, शादी-मैरिज जन्म-जन्मातर तो दूर की बात है वर्षों तक भी निभेगा अथवा नहीं ऐसा संदेह रहता है और इसी कारण उसमें तलाक-Divorce भी जुड़े हुये हैं।
वर्त्तमान में भी चाहे कितना भी दुःखी जीवन हो सनातनी जिसने विवाह किया होता है वो संबंध-विच्छेद नहीं करता है। किन्तु इसमें आप उन्हें सनातनी न कहें जो सनातनी होने का स्वांग मात्र करते हैं। शनैः-शनैः तलाक जैसी कुरीति धनाढ्य और नगरवासियों में प्रवेश कर गयी क्योंकि वो लोग अपने धर्म से दूर हो गये, अपनी संस्कृति को भुला बैठे। इसमें राजनीतिक कारण भी है और एक भाईचारा का जो षड्यंत्र चल रहा है वह भी है।
यदि शब्दों का महत्व नहीं होता है तो फिर मंत्रों, स्तोत्रों का महत्व कैसे सिद्ध होगा ? मंत्र-स्तोत्रादि तो शब्दों के समूह ही होते हैं न। यदि ये गिरोह कुछ वर्षों के पश्चात् मंत्र-स्तोत्रादि का भी अंग्रेजी, उर्दू, फ़ारसी आदि भाषाओं में रूपांतरण करके भी प्रयोग करने लगें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये उस श्रेणी के हैं जो अपनी मां को घर से भगा दे और वेश्याओं को मां बनाकर पूजे। ये पूजा किस प्रकार की होगी सभी समझ सकते हैं।
शब्द का महत्व भी होता है और प्रभाव भी होता है। जो लोग इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं उनके लिये मंत्रों-स्तोत्रों का भी कोई महत्व नहीं है, शास्त्रों का भी कोई महत्व नहीं है और उन्हें नास्तिक कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे जिसको देखने से, वार्तालाप करने से भी पाप लगता है उससे आप मेंहदी लगवाते हो, मेंहदी रस्म बोलते हो, शादी बोलते हो, थूका हुआ खाते हो और फिर पूजा-हवन करके दिखावा करते हो कि मैं धर्म कर रहा हूँ। ऐसा करके किसी और को नहीं अपनी आत्मा को नरक के मार्ग पर ले जाते हो।

शब्दों का महत्व होता है और प्रभाव भी होता है यदि न हो तो ये पंक्तियाँ शब्दों का ही समूह हैं और इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये तथापि वैसे लोगों को वज्रपात के समान लगेगा जिसके बारे में संकेत है। चूँकि शब्दों का महत्व होता है इस कारण रस्म, रिवाज़ आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, विवाह के स्थान पर शादी-मैरिज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, विवाह को अंग्रेजी में भी बोलना-लिखना हो तो Vivah ही रखना चाहिये।
आइये अब परम्परा और विधान को समझते हैं जो कि कर्मकांडियों के लिये ही नहीं जिनकी भी कर्मकांड और धर्म में रूचि हो सबके लिये महत्वपूर्ण है।
परम्परा और विधान
प्रायः लोगों को कहते देखा जाता है कि बाप-दादा करते आये हैं इसलिये कर रहा हूँ। वास्तव में यह परम्परा के प्रति ही है किन्तु विधान का ज्ञान न होने के कारण, धर्म-कर्मकांड में आस्था के अभाववश यह वचन उपनयन-विवाह-श्राद्ध आदि के लिये बोल दिया जाता है।
विधान और परम्परा को पृथक-पृथक करके समझना कठिन होगा इसलिये दोनों को संयुक्त रूप से ही समझना होगा। प्रायः विधान को भी परम्परा समझने की त्रुटि हो जाती है जिससे बड़ी हानि होती है और हानि का एक-दो उदाहरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है :
- प्रथम उदाहरण नित्यकर्म : नित्यकर्म विधान है किन्तु इसे परम्परा समझ लेने की कहीं न कहीं त्रुटि हुयी और इसका परिणाम यह है कि वर्त्तमान में मात्र 5-10 प्रतिशत कर्मकांडी ही नित्यकर्म करते हैं शेष नित्यकर्म विहीन हो चुके हैं। कर्मकांडी ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य की तो चर्चा ही क्या करें।
- द्वितीय उदाहरण वृद्धिश्राद्ध का लोप : वृद्धि श्राद्ध अर्थात नान्दी श्राद्ध बहुत अंशों में विलुप्त है और नित्यकर्म की तरह ही अत्यल्प क्षेत्रों में भी वृद्धि-श्राद्ध को विधान स्वीकार करते हुये किया जाता है।
- तृतीय उदाहरण संस्कार का लोप : हम देख रहे हैं कि सोलह संस्कारों में से अब मात्र मुंडन, उपनयन एवं औपचारिक रूप से वेदारंभ-समावर्तन, विवाह और अंतिम संस्कार इतने ही किये जाते है शेष संस्कारों का लोप हो चुका है और इसका मुख्य कारण संस्कारों को परम्परा मात्र समझने का भ्रम पाल लेना ही है।
विधान का तात्पर्य है शास्त्रों में वर्णित कर्म की विधि और यह परिवर्तनशील नहीं होता है, त्याज्य होना तो सोचा भी नहीं जा सकता। हां ये अवश्य है कि सबके लिये अभी कर्म अनिवार्य नहीं होता है। यथा अनेकों यज्ञ हैं किन्तु अनिवार्यता नहीं है सामर्थ्य होने पर भी करने की इच्छा हो तभी करे। लेकिन यदि करे तो जो यज्ञ करे उसके विधान का पालन करे। इसी प्रकार तीज और मधुश्रावणी के विषय में देखा जाता है तीज करने वाली मधुश्रावणी नहीं करती है और जो तीज नहीं करती है वह मधुश्रावणी करती है।
इसी प्रकार से रामनवमी, जन्माष्टमी आदि कुछ विशेष व्रत हैं जो अनिवार्य हैं, किन्तु सभी व्रत अनिवार्य नहीं होते। विभिन्न प्रकार के पूजा-अनुष्ठानों की अनिवार्यता नहीं होती, आवश्यक प्रतीत होने पर, इच्छा होने पर किया जाता है किन्तु जब किया जाये तो उसका विधान है जिसका पालन करना चाहिये। अब किसी धनाढ्य परिवार में प्रतिवर्ष रामार्चा करना आरंभ हो जाये तो अगली पीढ़ी को वह करना परम्परा प्रतीत होगा। उस परिवार के लिये रामार्चा करना परंपरा हो सकता है किन्तु रामार्चा परंपरा नहीं है इसका विधान है और विधान के अनुसार ही करना चाहिये।
इस प्रकार से किसी कर्म की शास्त्रों में जो विधि वर्णित हो वह विधान है, उसे परम्परा नहीं कहा जा सकता। कर्म की आवश्यकता और कर्तव्याकर्तव्य भिन्न विषय है। किन्तु जो कर्म किया जाये यदि वह शास्त्रोक्त है (परंपरा) नहीं है तो शास्त्रोक्त विधान का पालन करना आवश्यक होता है।
परम्परा पूर्वजों से प्राप्त वो विशेष कर्म-विधियां हैं जो विधान नहीं हैं, अर्थात शास्त्रोक्त नहीं हैं। इसे पारस्कर गृह्यसूत्र में ग्रामवचन कहा गया है, लोकाचार-कुलाचार-शिष्टाचार आदि भी कहा जाता है। किसी लोक व्यवहार (लोकाचार-कुलाचार-शिष्टाचार) की बारम्बारता परम्परा कही जाती है, अर्थात परंपरा का तात्पर्य उस लोकाचार-कुलाचार-शिष्टाचार को बारम्बार करते रहना अगली पीढ़ियों में भी करना परंपरा है।
इस बारम्बारता के सिद्धांत से ही कर्म भी परम्परा की श्रेणी में आ जाता है जैसे किसी परिवार में यदि प्रतिवर्ष रुद्राभिषेक किया जाने लगे तो वह अगली पीढ़ी को परम्परा लगेगी। किन्तु रुद्राभिषेक तो परम्परा नहीं है यह शास्त्रोक्त कर्म है, शास्त्र में इसकी विधि वर्णित है अर्थात यह रुद्राभिषेक का विधान है।
परम्परा एवं विधान में अंतर
इस विषय को और गहराई से समझने के लिये परम्परा एवं विधान में अंतर को समझना भी आवश्यक है :
धोती पहनना : धोती पहनना विधान है किन्तु इसे परम्परा-परम्परा करके ऐसी व्यवस्था बना दी गयी है कि अब तो विवाह-पूजा-पाठ में भी नये जमाने के शिक्षित-मूर्ख धोती नहीं पहनना चाहते हैं। यदि परम्परा होती तो परिवर्तन से कोई समस्या न होती किन्तु शास्त्र में धोती को धारण करने की विधि का भी त्रिकच्छ-पंचकच्छ आदि बताया गया है, सिले हुये वस्त्रों का शास्त्र में निषेध भी किया गया है। इस प्रकार पैंट-पैजामा आदि पहनकर धार्मिक कृत्य करना नहीं करने से अधिक भयावह है क्योंकि विधि का उल्लंघन करके किया जा रहा है।
किन्तु धोती में ही एक परंपरा जो वैष्णवों की भी देखी जाती है एवं दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है वो है लुंगी की भांति धारण करना। यह संप्रदाय विशेष, क्षेत्र विशेष की परंपरा है। यद्यपि इसके पीछे कारण है तथापि उन कारणों की चर्चा का उल्लेख करना यहां आवश्यक नहीं है।
वर्त्तमान युग में उत्पातियों ने ऐसी परिस्थियों का भी निर्माण कर रखा है कि यदि इस प्रकार की चर्चा करो तो कहेंगे उन्नीसवीं सदी का प्राणी है, इनको जमाने से पीछे चलने दो आप आगे बढ़ो। जमाने से पीछे चलने दो के संबंध में व्यापक चर्चा की आवश्यकता है जो एक बार पूर्व में की गयी है और आगे पुनः करेंगे। किन्तु पैंट और पैजामा नये जमाने का कैसे सिद्ध होता है जी, यह तो दूसरी संस्कृति का है जिसे नये जमाने का बनते हुये परम्परा बनाते जा रहे हो।
इसी प्रकार शिखा, चंदन-तिलक आदि को पंडितों का विषय बना दिया गया। यह सबके लिये शास्त्रोक्त विधान है। विवाह में कई प्रसंग हैं जिससे परंपरा और विधान का अंतर ज्ञात होता है :
विवाह में मंडप निर्माण करने का विधान है किन्तु मैथिल ब्राह्मणों में मंडप निर्माण नहीं होता है। इसका कारण प्राचीन काल में अधिकांश पकड़ौवा विवाह होना है। अचानक से वर का आगमन होने पर रात में न तो वृद्धिश्राद्ध किया जा सकता है और न ही मंडप निर्माण अतः वृद्धि श्राद्ध और मंडप निर्माण नहीं होने की परंपरा विकसित हो गयी किन्तु शास्त्रों में दोनों का विधान है। वर्त्तमान युग में जब पकड़ौवा विवाह नहीं होता है तब भी परम्परा को लेकर विधान का उल्लंघन करते रहना समीचीन नहीं है।
इसी प्रकार से विवाह में कंगन का विधान प्राप्त होता है किन्तु अठङ्गर का विधान प्राप्त नहीं होता अतः कंगन बंधन तो विधान है किन्तु अठङ्गर परंपरा। इसी प्रकार से कर्मकांड में सिर को वस्त्रादि से ढंकने का निषेध है अतः यह विधान है किन्तु विवाह में वर के लिये पगड़ी-मौड़ धारण की परंपरा है जो हवन करते समय भी देखी जाती है जबकि हवनकाल में पगड़ी-मौड़ नहीं होना चाहिये क्योंकि शास्त्र का विधान है।
इसी प्रकार से विवाह में लाजा होम का विधान है और अग्नि के चार प्रदक्षिणा का ही विधान है। किन्तु लाजा होम के स्थान पर लाजा बिखेरने की परम्परा विकसित हो गयी और चार परिक्रमा के स्थान पर सात फेरे की परंपरा।
इसी प्रकार से कहीं-कहीं विवाह-श्राद्ध आदि में बिल्ली को किसी डाला आदि से ढंका जाता है परम्परा है न कि विधान। किन्तु स्थिति यह होती है कि परंपरा के लिये विधान को भी तिलांजलि दे दिया जाता है जो कि अनुचित है। परम्परा पालन जितना हो ठीक है किन्तु परम्परा के कारण विधान का उल्लंघन न हो ध्यान रखना आवश्यक होता है।
उपनयन में व्रात्य हेतु शिखा वपन की एक विशेष विधि है, किन्तु जो व्रात्य नहीं हैं उनके लिये शिखा स्थापन का विधान है जिसे चूड़ाकरण (मुंडन) कहा जाता है। किन्तु जब व्रात्यों का शिखा वपन होने लगा तो किसी न किसी भ्रमवश जो व्रात्य नहीं होते उनका भी शिखा स्थापन के स्थान पर शिखा वपन करने की परंपरा विकसित हो गयी जो उचित नहीं है।
निष्कर्ष : इस आलेख में शब्द का महत्व स्पष्ट करते हुये यह बताया गया है कि रीति-परंपरा-प्रथा-विधि-विधान आदि शब्दों के स्थान पर रस्म-रिवाज़ जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसी प्रकार से विवाह के लिये शादी-मैरिज आदि शब्दों का प्रयोग करना भी अनुचित है। इसके साथ ही परम्परा और विधान के संबंध में उदाहरण सहित विस्तृत चर्चा की गयी है एवं परम्परा और विधान के अंतर को गंभीरता से समझने के लिये दोनों के पर्याप्त उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं।
विनम्र आग्रह : त्रुटियों को कदापि नहीं नकारा जा सकता है अतः किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि दृष्टिगत हो तो कृपया सूचित करने की कृपा करें : info@karmkandvidhi.in
कर्मकांड विधि में शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ प्रामाणिक चर्चा की जाती है एवं कई महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा पूर्व भी की जा चुकी है। तथापि सनातनद्रोही उचित तथ्य को जनसामान्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक बड़ा वैश्विक समूह है जो सनातन विरोध की बातों को प्रचारित करता है। गूगल भी उसी समूह का सहयोग करते पाया जा रहा है अतः जनसामान्य तक उचित बातों को जनसामान्य ही पहुंचा सकता है इसके लिये आपको भी अधिकतम लोगों से साझा करने की आवश्यकता है।
Discover more from कर्मकांड सीखें
Subscribe to get the latest posts sent to your email.